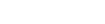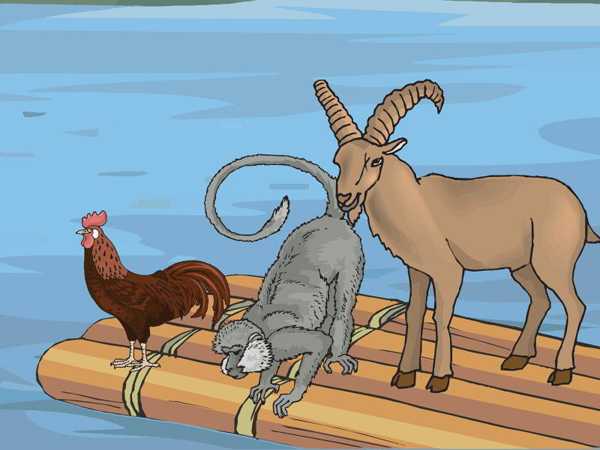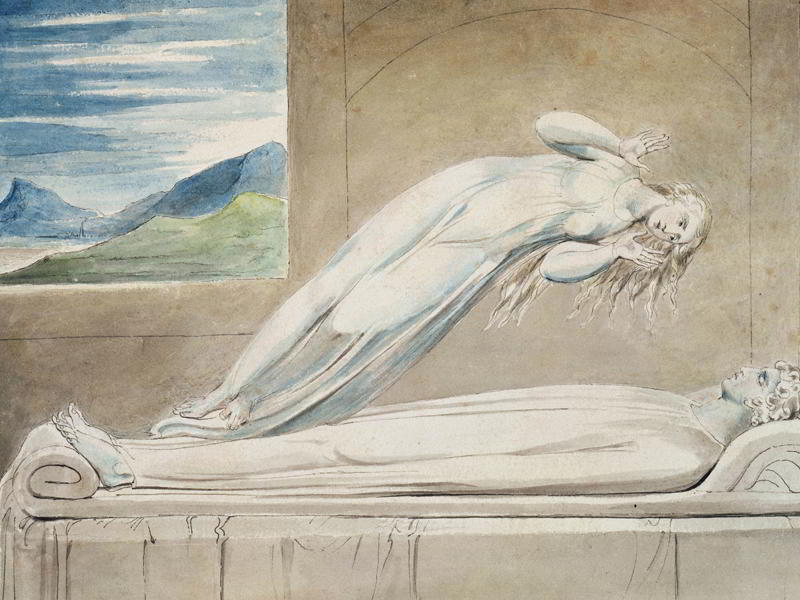फिर कभी जलेबी मत माँगना

ज़िक्र है कि एक मुसलमान फ़क़ीर एक दिन बाज़ार से गुज़र रहा था| रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी| उसने बड़ी अच्छी जलेबियाँ सजाकर रखी हुई थीं| मन ने कहा, जलेबियाँ खानी हैं| पास पैसा था नहीं, करे तो क्या करे| मन को समझाया-बुझाया, लेकिन मन न माना| आख़िर वहाँ से वापस चला आया|
मन की आदत है कि इसको जिस तरफ़ से मोड़ो उधर ही जाता है| जब रात को भजन में बैठा तो जलेबियाँ सामने| मन बाहर जाने लगा| फ़क़ीर उठ गया| जब फिर बैठा, फिर वही ख़याल सामने आया| जब सुबह हुई तो वह पैसे कमाने के लिए काम करने गया| गर्मी बहुत थी और उसका मालिक बहुत कड़े स्वभाव का था| जैसे-जैसे शाम को थककर चूर होकर लड़खड़ाता हुआ बाज़ार आया क्योंकि उसका मन जलेबियाँ खाना चाहता था|
उस समय जलेबियाँ सस्ती थीं| रुपये की तीन सेर होती थीं| तीन सेर जलेबियाँ ख़रीदीं और जंगल में ले गया| कुछ खायीं, पेट भर गया| मन से कहा कि और खा| और खायीं, आख़िर मन ने मुँह फेर लिया| फिर बोला कि और खा| और खायीं तो उलटी हो गयी| जब उलटी हो गयी तो मन को हुक्म दिया कि अब इस उलटी को भी खा| आख़िर हारकर मन ने कहा कि फिर कभी जलेबियाँ नहीं माँगूँगा|
सो मन बातों से वश में नहीं आता|